अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस

“महिला सुरक्षा" को सुनिश्चित करने वाले महिला कानूनों को जानिए!
हर साल 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं को समाज में बराबरी और लोगों को उनके अधिकारों को लेकर जागरूक करने के मकसद से मनाया जाता है। महिलाओं की सुरक्षा और विकास के लिए हमारे भारत में अनेकों कानून है जिनका मकसद समाज में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो आइए जानते हैं कुछ प्रमुख महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में।
महिलाओं को संविधान ने दिए 6 कानून
बरसों से हमारे समाज का एक तबका महिलाओं को समाज और देश निर्माण के लिए अवांछनीय बताता रहा है और उन्हें निर्बल रखना ही बेहतर समझता आया है। उनके मुताबिक एक महिला की अपनी कोई इच्छा या सपने नहीं होने चाहिए। उनके हिसाब से महिलाओं की जिम्मेदारी समाज और परिवार की जरूरतों को पूरा करना ही है। ऐसे में जो महिलाएं समाज में आगे बढ़ना चाहती हैं उन महिलाओं के साथ कदम कदम पर पक्षपात किया जाता है और उन्हें अपने अधिकार के प्रति लड़ने की आजादी तक नहीं होती। यहां हम ऐसी महिलाओं को उनकी ताकत और अधिकार की जानकारी दे रहे हैं जिसकी मदद से वे अपने साथ हो रहे भेदभाव या अत्याचार से खुद को सुरक्षित कर सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं।
दफ्तर में यौन हिंसा और प्रताड़ना के विरोध में कानून
कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की यौन हिंसा और प्रताड़ना से स्त्रियों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए पॉश– द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रीड्रेसल बेनिफिट एक्ट, 2013) कानून बनाया गया है। 3 सितंबर, 2012 को यह लोकसभा से और 26 फरवरी, 2013 को राज्यसभा से पारित हुआ और 9 दिसंबर, 2013 से यह कानून प्रभाव में आया। इस कानून के तहत कोई भी सरकारी या गैरसरकारी दफ्तर, जहां 10 से ज्यादा कर्मचारी हैं और जहां महिलाएं काम करती हैं, वहां पॉश कमेटी बनाना अनिवार्य कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में एक वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट (Workplace Sexual Harassment) केस के बाद स्वत: संज्ञान लेते हुए यह गाइडलाइंस जारी की थीं। वह केस दरअसल भंवरी देवी का था जो एक एनजीओ में काम करती थीं। काम के दौरान उनके साथ रेप हुआ था। कानून के तहत ऑफिस में काम कर रही महिला की सुरक्षा को सुनिश्चित करना संस्थान की जिम्मेदारी है और यदि उनके साथ कोई भी अनुचित व्यवहार होता है तो वो शिकायत कर सकती हैं।
पिता की संपत्ति को लेकर महिलाओं का अधिकार
आजाद भारत में महिलाओं के लिए लाया गया सबसे ऐतिहासिक और सबसे जरूरी कानून है हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू उत्तराधिकार कानून (2005)। हालांकि, ऐसा कानून 1956 के नाम से पहले भी था। लेकिन उसमें लड़के और लड़की के लिए भेदभावपूर्ण नियम थे। उस कानून में लड़कियों का पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। पिता की सारी संपत्ति लड़कों को मिलती थी। 2005 में इस कानून में संशोधन किया गया और 9 सितंबर, 2005 में यह लागू हुआ। नए कानून में पुराने लैंगिक भेदभाव को खत्म किया गया और बड़ा फैसला सुनाया गया। न्यायालय ने पैतृक संपत्ति में भी लड़कियों को बराबर का अधिकार देने की घोषणा की। समान संपत्ति का अधिकार अब तक सिर्फ पिता की अर्जित की हुई संपत्ति पर ही लागू होता था। पैतृक संपत्ति अब भी स्वत: ही बेटों की होती थी। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक पैतृक संपत्ति में भी बेटे और बेटी को बराबर का अधिकार सुनिश्चित किया गया।
अबॉर्शन का अधिकार
किसी भी महिला के पास अबॉर्शन का अधिकार होता है यानी वह चाहे तो अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को अबॉर्ट कर सकती है। इसके लिए उसे अपने पति या ससुरालवालों के सहमति की जरूरत नहीं है। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 (The Medical Termination of Pregnancy Act, 1971) के तहत ये अधिकार दिया गया है कि अगर प्रेग्नेंसी 24 सप्ताह से कम है तो एक महिला अपनी प्रेग्नेंसी को किसी भी समय खत्म कर सकती है। स्पेशल केसेज़ में एक महिला अपने प्रेग्नेंसी को 24 हफ्ते के बाद भी अबॉर्ट करा सकती है।
मातृत्व अवकाश
यह कानून हर कामकाजी महिला के लिए छह महीने के मातृत्व अवकाश को सुनिश्चित करता है। यह उसके नौकरी के अधिकार और मातृत्व अवकाश के दौरान पूरी सैलरी को सुनिश्चित करता है। यह कानून हर उस सरकारी और गैरसरकारी कंपनी पर लागू होता है, जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं।
मैटर्निटी बेनिफिट (एमेंडमेंट) बिल या मातृत्व लाभ (संशोधन) बिल 11 अगस्त, 2016 को राज्य सभा और 9 मार्च, 2017 को लोकसभा में पास हुआ। 27 मार्च, 2017 को यह कानून बना। हालांकि मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961 में ही लागू हुआ था, लेकिन तब अवकाश सिर्फ तीन महीने का हुआ करता था। 2017 में इसे बढ़ाकर छह महीने कर दिया गया।
डिस्क्लेमर:
ऊपर व्यक्त विचार लेखक के निजी हैं और ये आवश्यक रूप से आजादी.मी के विचारों को परिलक्षित नहीं करते हैं।



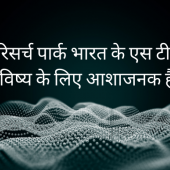





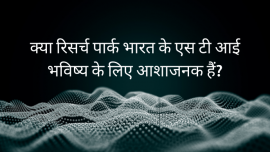




Comments